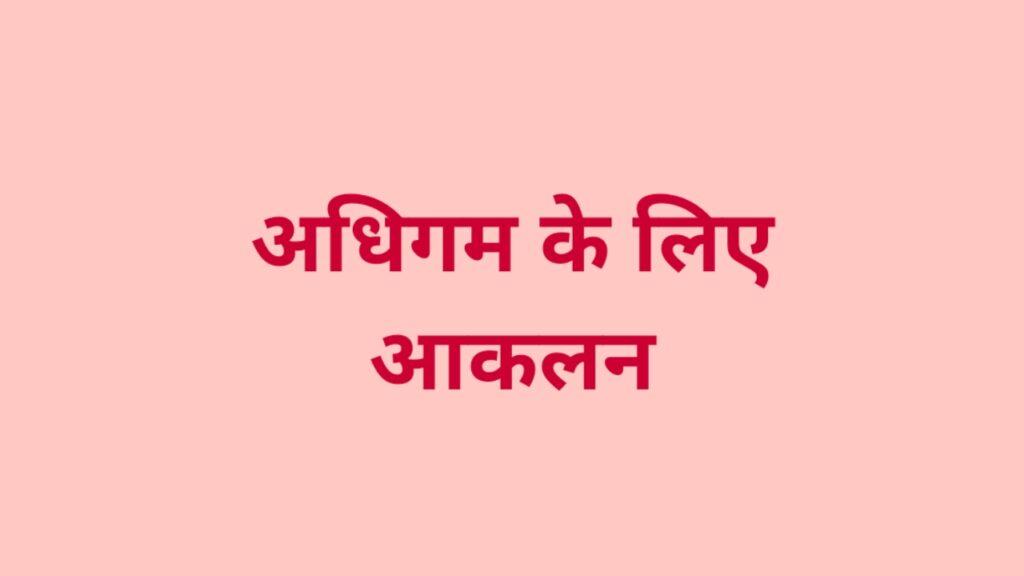अधिगम के लिए आकलन एक प्रणाली और प्रक्रिया है जो छात्रों में सीखने का मूल्यांकन एक साथ होती है। इसका उपयोग कहीं भी सीखने के लिए किया जाता है, चाहे वह शिक्षा का स्थान हो या कार्य का स्थान हो। एस्टीमेट विद्यार्थियों को उनकी शिक्षण पद्धतियों की प्रगति के बारे में और संकाय प्रदान करता है और उनके शिक्षण पद्धतियों को एस्टीमेट्स में मदद करता है। वे विद्यार्थियों को उनके द्वारा दिए गए ग्रेड के लिए आवश्यक मानक के रूप में भी कार्य करना पड़ता है।
आकलन की एक अच्छी प्रणाली सीखने के लिए परिभाषा से शुरू होती है। इन विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक लक्ष्य तक के लिए सीधे लक्ष्य शिक्षण प्रशिक्षण और परीक्षण शामिल हैं।
मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध से परीक्षण, स्मृति और सीखने के बीच बातचीत का पता लगाया जाता है। यह सुझाव देता है कि एक मूल्यांकन प्रक्रिया जो एक छात्र ने उसे रखी है उसे बनाए रखने में मदद मिल सकती है और विभिन्न संदर्भों को सीखने में लागू करने में भी मदद मिल सकती है।
आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ज्ञात उद्देश्य या लक्ष्य के सापेक्ष जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके अलावा, यह एक बड़ा शब्द है जिसमें परीक्षण भी शामिल है। इसी प्रकार परीक्षण भी आकलन का ही एक रूप है। इसके अलावा, परीक्षण अप्राकृतिक परिस्थितियों में किए गए आकलन के प्रबंधन के लिए होते हैं।
दूसरे शब्दों में, आकलन प्रदर्शन को मापने की एक प्रक्रिया है। यह छात्रों के ज्ञान का भी परीक्षण करता है। इस कारण से, सभी परीक्षण आकलन हैं लेकिन सभी मूल्यांकन परीक्षण नहीं हैं। इसके अलावा, वे पाठ या इकाई के अंत में परीक्षण आयोजित करते हैं।
आकलन का आशय है- सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करता है।
आकलन की प्रक्रिया में Assessment Performance Test का प्रयोग किया जाता है और आकलन में छात्रों को बिना अंक अथवा ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है ताकि शैशिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक मूल्याकल के पूर्व सुधार सभव हो सके।
यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है. जिससे हम परीक्षण के माध्यम से छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करते हैं। इसके अलावा, वे छात्रों के कौशल ज्ञान और दृष्टिकोण से संबंधित डेटा एकत्र करने में मदद करते हैं। इसके अलावा, वे छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।
नोट – हमारी वेबसाइट पर B.Ed प्रोग्राम के लगभग सभी टॉपिको पर विस्तारपूर्वक विशेषण किया गया है, यह विश्लेषण आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है जिसके लिए आपको मेनू में जाकर B.Ed प्रोग्राम को सेलेक्ट करके देख सकते हैं।
“आकलन में कार्यक्रमों को परिष्कृत करने और छात्रों के सीखने में सुधार करने के लिए छात्र के सीखने पर प्रयोगात्मक डेटा का उपयोग शामिल है।” – एलन
आकलन द्वारा विद्यार्थी को अधिकतम क्षमता को बढ़ाने मूल्यांकन के पहले सुधार हेतु पृष्ठ पोषण किया जाता है। यह मूल्यांकन का ही एक छोटा रूप होता है इसके शैशिक्ष महत्व काफी ज्यादा है जो अधिगम के लिए गुणात्मकपूर्ण वातावरण निर्मित करने के लिए अति आवश्यक होता है।
आकलन सीखने की प्रक्रिया से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार यह अध्ययन एवं अध्यापन के क्रम से जुड़ जाता है। छात्रों की प्रगति और उपलब्धि पर नज़र रखने के लिए अध्ययन का पाठ्यक्रम निरंतर भूमिका निभाता है। साथ ही, शिक्षक और छात्र अध्ययन के पाठ्यक्रम के परिणामों को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं।
कक्षा समीक्षा से शिक्षकों को छात्रों के सीखने का लगातार पता लगाने में मदद मिलती है। यह छात्रों को एक छात्र के रूप में उनके सुधार की गणना देता है। सीखने की प्रक्रिया में छात्रों को करीबी परीक्षा का मौका प्रदान करता है।
वे छात्रों की सीखने की नियमित प्रतिक्रिया के संग्रह में मदद करते हैं। साथ ही, वे विशिष्ट शिक्षण दृष्टिकोणों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यह विभिन्न प्रकार की योजनाओं का उपयोग करता है। राय का विद्यार्थियों के स्वाभिमान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही यह सीखने के लिए भी खतरनाक है।
इस प्रकार, आकलन में शिक्षकों की वे सभी गतिविधियाँ शामिल होती हैं जो छात्रों की समीक्षा करने में मदद करती हैं। इसके अलावा, यह जानकारी समीक्षा के रूप में उपयोग की जाती है और शिक्षण गतिविधि को संशोधित करती है।
(1) आकलन निर्देश को प्रेरित करता है
एक पूर्व-परीक्षण या आकलन की आवश्यकता प्रशिक्षकों को सूचित करती है कि छात्र शुरुआत में क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं, जिससे पाठ्यक्रम की दिशा निर्धारित होती है। यदि अच्छी तरह से किया जाए, तो प्राप्त जानकारी मौजूदा ज्ञान और वांछित परिणाम के बीच अंतर को उजागर करेगी। निपुण प्रशिक्षक यह पता लगाते हैं कि छात्र पहले से क्या जानते हैं, और नई समझ विकसित करने के लिए पूर्व ज्ञान को एक कदम के रूप में उपयोग करते हैं। निर्देश के दौरान किए गए मूल्यांकन के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के लिए भी यही सच है। पूरे शिक्षण के दौरान छात्रों से बातचीत करके, उत्कृष्ट प्रशिक्षक छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने शिक्षण को लगातार संशोधित और परिष्कृत करते हैं।
(2) आकलन सीखने को प्रेरित करता है
छात्र क्या और कैसे सीखते हैं यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि वे कैसे सोचते हैं कि उनका आकलन किया जाएगा। आकलन प्रथाओं को छात्रों को क्या अध्ययन करना है, कैसे अध्ययन करना है और पाठ्यक्रम में अवधारणाओं और कौशल पर खर्च करने के लिए सापेक्ष समय के बारे में सही संकेत भेजना चाहिए। निपुण संकाय स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं कि छात्रों को क्या जानने और करने में सक्षम होने की आवश्यकता है, दोनों स्पष्ट रूप से व्यक्त पाठ्यक्रम के माध्यम से, और छात्र ऊर्जा को निर्देशित करने के लिए सावधानीपूर्वक मूल्यांकन का चयन करके। जो छात्र इस अवसर पर खरे उतरते हैं उनमें सीखने के परिणाम को लेकर उच्च उम्मीदें होती हैं।
(3) आकलन छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में सूचित करता है
प्रभावी आकलन छात्रों को यह एहसास कराता है कि वे किसी विषय के बारे में क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। यदि अच्छा किया जाए, तो छात्रों को प्रदान किया गया फीडबैक उन्हें संकेत देगा कि वे अपने प्रदर्शन को कैसे सुधारें। मूल्यांकन स्पष्ट रूप से कक्षा में सिखाई गई सामग्री, सोच की प्रकृति और कौशल से मेल खाना चाहिए। प्रशिक्षकों के फीडबैक के माध्यम से, छात्र पाठ्यक्रम सीखने के परिणामों के संबंध में अपनी ताकत और चुनौतियों से अवगत हो जाते हैं। अच्छे से किया गया मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए।
(4) आकलन शिक्षण अभ्यास को सूचित करता है
छात्र उपलब्धियों पर प्रतिबिंब प्रशिक्षकों को उनकी शिक्षण रणनीतियों की प्रभावशीलता पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। साक्ष्यों को व्यवस्थित रूप से इकट्ठा करने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने से हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि किसी पाठ, इकाई या पाठ्यक्रम के लिए छात्रों की शिक्षा हमारे परिणामों/अपेक्षाओं से कितनी अच्छी तरह मेल खाती है। फीडबैक से प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षक को इंगित करता है कि निर्देश को कैसे सुधारना है, शिक्षण को कहाँ मजबूत करना है, और कौन से क्षेत्र अच्छी तरह से समझे जाते हैं और इसलिए भविष्य के पाठ्यक्रमों में कटौती की जा सकती है।
(5) आकलन में ग्रेडिंग की भूमिका
ग्रेड इस बात का प्रतिबिंब होना चाहिए कि छात्र ने क्या सीखा है, जैसा कि छात्र के सीखने के परिणामों में परिभाषित किया गया है। उन्हें छात्रों के सीखने के प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित होना चाहिए जैसा कि परीक्षणों, कागजात, परियोजनाओं और प्रस्तुतियों आदि पर मापा जाता है। ग्रेड अक्सर हमें “बड़े सीखने” जैसे कि महत्वपूर्ण सोच कौशल, समस्या सुलझाने की क्षमता, संचार कौशल (मौखिक, लिखित और सुनना), सामाजिक कौशल और भावनात्मक प्रबंधन कौशल के बारे में स्पष्ट रूप से बताने में विफल होते हैं।
(6) जब विद्यार्थियों के सीखने के परिणाम पूरे नहीं होते
निपुण संकाय पाठ्यक्रम के पहले, उसके दौरान और अंत में उनके द्वारा पूरे किए गए मूल्यांकन से आने वाले डेटा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और यह निर्धारित करते हैं कि छात्रों के सीखने के परिणाम किस हद तक पूरे होते हैं या नहीं। यदि छात्र शुरुआत में ही पाठ्यक्रम से भटक जाते हैं, तो किसी विषय को पुनर्निर्देशित करना, छात्र शिक्षण केंद्रों का संदर्भ देना, या प्रशिक्षक द्वारा समीक्षा सत्र से समस्या का समाधान हो सकता है। सावधानीपूर्वक विश्लेषण के माध्यम से छात्रों को बेहतर सीखने में सहायता करने के लिए निर्देश की चुनौतियों और कमजोरियों को निर्धारित करना संभव है। कुछ विषय या अवधारणाएँ बेहद कठिन हैं, और उनका उपयोग करने के लिए एक बेहतर दृष्टिकोण हो सकता है। शायद एक मॉडल, सिमुलेशन, प्रयोग, उदाहरण या चित्रण छात्रों के लिए अवधारणा को स्पष्ट करेगा। शायद थोड़ा और समय बिताने से, या किसी विषय पर दूसरे तरीके से विचार करने से फर्क पड़ेगा।
आकलन की आवश्यकता बिद्यालय में अध्यापन के पश्चात छात्रों की अधिगम क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व अभियोग्यता आदि के बारे में जानकारी करने तथा उनके अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण के लिए आकलन की आवश्यकता पड़ती है।
अधिगम में जब तक छात्रों को feedback प्राप्त नहीं होते हैं तब तक यह प्रणाली प्रभावशील नहीं होती है। जब वे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और क्या उन्होंने जानकारी प्राप्त कर ली है, वह क्या जान चुके हैं, इस अधिगम की प्रक्रिया में प्राप्त जानकारी एवं ज्ञान को आकलन के द्वारा मापा जाता है। आकलन को मुख्य दो तीन रूप में मापा जाता है।
(1) स्वयं आकलन
इस आकलन में छात्र कक्षा अध्यापन के माध्यम से सीखते हैं तथा अपने अधिगम का मूल्यांकन करते हैं। यह पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि जो छात्र स्नातक, b.ed छात्राध्यापक है वह स्वयं के कार्य को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देख कर स्वयं की कमियों को जानने का प्रयास करते हैं तथा उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं।
(2) सहपाठी या सहयोगी समूह (Peer assessment)
जो छात्र अपने सहपाठियों या अन्य छात्रों से अधिगम के दौरान फीडबैक प्रदान करते हैं। यह आकलन सहपाठी आकलन कहलाता है। यह आकलन स्वयं आकलन से ज्यादा विस्तृत होता है।
(3) टयूटर आकलन
जब शिक्षक आकलन करते हैं तो उसे ट्यूटर आकलन कहते हैं। इसमें टयूटर या शिक्षक छात्र के कार्यों पर उस ए फीडबैक प्रदान करते हैं।
- विश्वास रिपोर्ट
यह आकलन की एक पारंपरिक पद्धति है. आम तौर पर, सरकारी संगठन इसका उपयोग आकलन के लिए करते हैं। स्टाफ़ का स्टाफ़ वयोवृद्ध यह रिपोर्ट तैयार करता है। इसमें स्टाफ की ताकतें और कमजोरियां, मुख्य उपलब्धियां और असफलताएं आदि शामिल हैं।
इसलिए, यह कर्मचारियों की मोटरसाइकिल और शोरूम के लिए एक विवरणात्मक रिपोर्ट बन जाती है। इस तकनीक का एक नुकसान डेटा के बजाय इंप्रेशन पर इसकी शुरुआत है। यह कार्यप्रणाली कर्मचारियों के विकास के बजाय मूल्यांकन पर केंद्रित है।
- सीधी रैंकिंग पद्धति
इस तकनीक में, मूल्यांकनकर्ता एक ही कार्य इकाई में समान कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को सापेक्ष रैंक प्रदान करता है। मूल्यांकनकर्ता कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अच्छे से बुरे तक रैंक प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि पांच व्यक्तियों A, B, C, D और E को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक मिलती है, तो यह इस प्रकार होगी।
- युग्मित तुलना विधि
मूल्यांकन की यह पारंपरिक पद्धति सीधी रैंकिंग पद्धति का एक संशोधन है। इस पद्धति के तहत, सीधी रैंकिंग पद्धति के विपरीत, सभी कर्मचारियों की सापेक्ष तुलना की जाती है। तुलना के बाद कर्मचारी को उसकी स्थिति अन्य कर्मचारियों से बेहतर होने के आधार पर रैंक मिलती है।
- जबरन वितरण प्रणाली
इस तकनीक में, मूल्यांकनकर्ता अपनी रेटिंग को सामान्य आवृत्ति वितरण के रूप में वितरित करता है। इसका मूल उद्देश्य मूल्यांकनकर्ता की केन्द्रीय प्रवृत्ति के पूर्वाग्रह को समाप्त करना है। इस विधि को लागू करना और समझना बेहद आसान है। इस पद्धति का एक नुकसान यह है कि मूल्यांकनकर्ता यह नहीं बता सकता कि कोई कर्मचारी किसी विशेष श्रेणी में क्यों है।
- ग्राफिक रेटिंग स्केल
यह एक संख्यात्मक पैमाना है जो किसी विशेष गुण की विभिन्न डिग्री बताता है। इस पद्धति के तहत, कंपनी या संगठन प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता को एक फॉर्म प्रदान करता है। प्रत्येक फॉर्म में कर्मचारी के व्यक्तित्व और प्रदर्शन से संबंधित कई विशेषताएं शामिल होती हैं। इसलिए, मूल्यांकनकर्ता पैमाने पर कर्मचारी की विशेषता पर अपना निर्णय दर्ज करता है।
- चेकलिस्ट विधि
यह मूल्यांकन के पारंपरिक तरीकों में से एक है। एक चेकलिस्ट और कुछ नहीं बल्कि बयानों की एक सूची है जो काम पर कर्मचारियों की विशेषताओं और प्रदर्शन का वर्णन करती है। मूल्यांकनकर्ता यह बताने के लिए टिक/चेक करता है कि कर्मचारी में कोई विशिष्ट गुण/गुण है या नहीं। इसलिए, टिक की संख्या कर्मचारी की रेटिंग या परिणाम का वर्णन करती है।
मूल्यांकन का अर्थ (Meaning of Evaluation)
शैक्षिक मूल्यांकन छात्रों के मूल्यांकन को व्यक्त करता है जिसमें छात्रों का बौद्धिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किया जाता है शिक्षा में मूल्यांकन एक नवीन अवधारणा है इसका प्रयोग विद्यालय कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री आदि की जांच के लिए किया जाता है मूल्यांकन प्रचलित परीक्षाओं की तुलना में बहुत अधिक व्यापक तथा उद्देश्यपूर्ण है परीक्षा की तरह मूल्यांकन में एक या दो बार की जांच से कार्य नहीं चलता मूल्यांकन की प्रक्रिया एक सतत प्रयास है, जिसके द्वारा अध्यापक और विद्यार्थियों दोनों अपने परिश्रम तथा लाभ की मात्रा का मूल्यांकन करते हैं।
मूल्यांकन की परिभाषा (Definition of Evaluation)
मूल्यांकन की परिभाषाएं निमंलिखित हैं-
- ब्रेडफील्ड एवं मोरडोक के अनुसार, “मूल्यांकन किसी घटना को प्रतीक आवष्टित करना है जिससे उस घटना का महत्त्व अथवा मूल्य किसी सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदण्ड के सन्दर्भ में ज्ञात किया जा सके।”
- एच० एच० रैमर्स तथा एम० एल० गेज के अनुसार, “मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज अथवा दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है अथवा क्या वांछनीय है का विस्तार निहित रहता है।”
- एन० एम० डाण्डेकर के अनुसार, “मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सोमा ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।”
मूल्यांकन के उद्देश्य (Objectives of Evaluation)
- छात्रों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करना
मूल्यांकन छात्रों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। छात्र मूल्यांकन के माध्यम से अपनी प्रगति के बारे में जान पाते हैं और अपने विकास का प्रयास करते हैं। छात्र को जिस क्षेत्र में अपने विकास में कमी लगती है वह उस क्षेत्र के विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करता है। इस प्रकार उसका चतुर्मुखी विकास सम्भव हो पाता है।
- छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान की जाँच करना
मूल्यांकन द्वारा छात्र ने जिस ज्ञान को अर्जित किया है, वह कितना उपयोगी है तथा छात्र उसके माध्यम से अपना कितना विकास कर पाया है इस बात की जाँच मूल्यांकन के माध्यम से ही होना सम्भव है।
- छात्रों की वृद्धि तथा विकास में उत्पन्न अवरोधों को जानना
मूल्यांकन का एक उद्देश्य यह भी है कि छात्रों की वृद्धि तथा विकास के मार्ग में कौन-कौन से अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। उन परेशानियों को चिह्नित करना तथा उन्हें दूर करना। बालक का सर्वतोमुखी विकास तभी सम्भव है जब उसे अपनी बुद्धि एवं विकास के मार्ग की रुकावटों की जानकारी होगी और यह कार्य मूल्यांकन करता है।
- छात्रों की शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्त्वों को जानना
मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों की शैक्षिक प्रगति में आने वाले बाधक तत्त्वों का जान हो जाता है जिसके फलस्वरूप भविष्य में छात्र उन बाधक तत्त्वों को दूर करने का प्रयास करता है, निरन्तर अभ्यास करता है, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। अतः मूल्यांकन का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्त्वों को जानना भी है। छात्रों को सोखने सम्बन्धी कठिनाइयों तथा कमजोरियों का ज्ञान होना आवश्यक है। मूल्यांकन की तकनीकी के प्रयोग से छात्रों की सोखने सम्बन्धी तत्त्वों को जानकर उन समस्याओं का निदान किया जाता है जो छात्र की शैक्षिक प्रगति में बाधक होते हैं।
- छात्रों में प्रतियोगिता की भावना विकसित करना
मूल्यांकन का एक उद्देश्य छात्रों में प्रतियोगिता की भावना विकसित करना भी है। छात्र प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं तथा अपना चतुर्मुखी विकास करना चाहते हैं। इस प्रकार मूल्यांकन छात्रों में प्रतियोगिता की भावना के द्वारा उनका विकास करने का प्रयास करता है।
- छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी करना
मूल्यांकन का एक उद्देश्य छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानना भी है। कुशाग्र एवं मन्द बुद्धि छात्रों में भेद करने के लिए, अच्छी योग्यता एवं कम योग्यता के छात्रों में अन्तर करने के लिए हमें छात्रों की बुद्धि एवं योग्यता की विभिन्नताओं का मूल्यांकन करना आवश्यक होगा।
- छात्रों का चयन एवं वर्गीकरण करना
मूल्यांकन का एक उद्देश्य छात्रों का चयन एवं वर्गीकरण करना भी है। कक्षा शिक्षण करते समय छात्रों के बौद्धिक स्तर के आधार पर उनका चयन प्रतिभाशाली, सामान्य स्तर तथा मन्द बुद्धि के स्तर के छात्रों के रूप में जानना तथा उसी प्रकार वर्गीकरण के आधार पर छात्रों को शिक्षण देने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है।
- कक्षोन्नति व रोजगार के लिए शैक्षिक योग्यता का प्रमाण
पत्र देना-कक्षोन्नति एवं रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। यह प्रमाण पत्र छात्रों को उनके मूल्यांकन के आधार पर ही वितरित किये जाते है जिसमें छात्रों को ग्रेड तथा नम्बर आदि लिखे होते हैं जो कि प्राप्त शैक्षिक योग्यता का प्रमाण होते हैं अतः इन सभी के लिए मूल्यांकन को आवश्यकता होती है।
- शैक्षिक मानकों का निर्धारण करना
मूल्यांकन के आधार पर ही शैक्षिक मानको का निर्धारण किया जाता है। जिस आधार पर छात्रों का स्तर तथा ग्रेड दिये जाते हैं उसी आधार पर प्रमाण-पत्र भी वितरित किये जाते है। बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य, मन्द बुद्धि के आधार पर ही मानक निश्चित किये जाते हैं। शैक्षिक निष्पत्ति में छात्र का स्तर क्या है यह इन मानकों के आधार पर ही पता चलता है।
- छात्रों के शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन के लिए आधार तैयार करना
मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों के शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन के लिए आधार तैयार किया जाता है। मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक दिशा निर्देशन भी दिया जाता है। छात्र जिस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता है उस क्षेत्र में उसकी सफलता की अधिक सम्भावना आँकी जाती है।
मूल्यांकन के प्रकार (Types of Evaluation)
मूल्यांकन को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-
जब कोई भी शैक्षिक योजना अपनी प्रारम्भिक या निर्माणावस्था में हो और उसका मूल्यांकन कर उसमें सुधार किया जा सके एवं उसकी प्रभावशीलता, गुणवत्ता, वांछनीयता या उपयोगिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है तो इस प्रकार के मूल्यांकन को संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी शैक्षिक योजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व उसका मूल्यांकन कर उसमें सुधार करने की प्रक्रिया को ही संरचनात्मक मूल्यांकन कहकर पुकारते हैं। उदाहरणार्थ, यदि किसी शोध योजना के प्रथम प्रारूप का मूल्यांकन इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि उसे प्रस्तुत करने और उस पर क्रियान्वयन करने से पूर्व उसमें वांछित सुधार कर उसे अधिक प्रभावशाली बनाया जाए तो इस प्रकार के मूल्यांकन को हम संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं तथा मूल्यांकन की यह भूमिका संरचनात्मक भूमिका कहलाती है।
संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा तैयार की गई योजना की कमियों को इंगित करना तथा उसमें सुधार के उपाय बताना होता है। इस दृष्टिकोण में संरचनात्मक मूल्यांकनकर्ता के कार्य को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, शैक्षिक कार्यक्रम या योजना के गुण-दोषों के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण जुटाना द्वितीय, इन प्रमाणों के आधार पर कार्यक्रम की कमियों को सामने रखना; तृतीय, इन कमियों को दूर करके कार्यक्रम को अधिक प्रभावकारी रूप देने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।
किसी शैक्षिक कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे देने को एवं उसे चालू कर देने के पश्चात् उसकी समानता को ज्ञात करने के लिए किया गया मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि उस योजना या कार्यक्रम को चालू रखा जाए या नहीं। स्पष्टता योगात्मक मूल्यांकन का अभिप्राय पहले से चल रही योजना को जारी रखा जाए या नहीं का निर्णय लेना होता है। इसके अतिरिक्त अनेक वैकल्पिक कार्यक्रमों में से किसको जारी रखा जाए और किसको छोड़ दिया जाए इस उद्देश्य की प्राप्ति योगात्मक मूल्यांकन द्वारा की जाती है।
उदाहरणार्थ, यदि एक अध्यापक को अपने छात्रों को किसी विषय के लिए कोई पुस्तक बतानी है और वह उस विषय पर उपलब्ध अनेक पुस्तकों में से मूल्यांकन कर कोई एक पुस्तक उन्हें बताता है तो शिक्षक का यह मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि योगात्मक मूल्यांकन द्वारा अनेक विकल्पों में से सर्वोत्तम चयन करने की प्रक्रिया है परन्तु इस सर्वोत्तम का चयन विकल्पों के गुण-दोषों के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
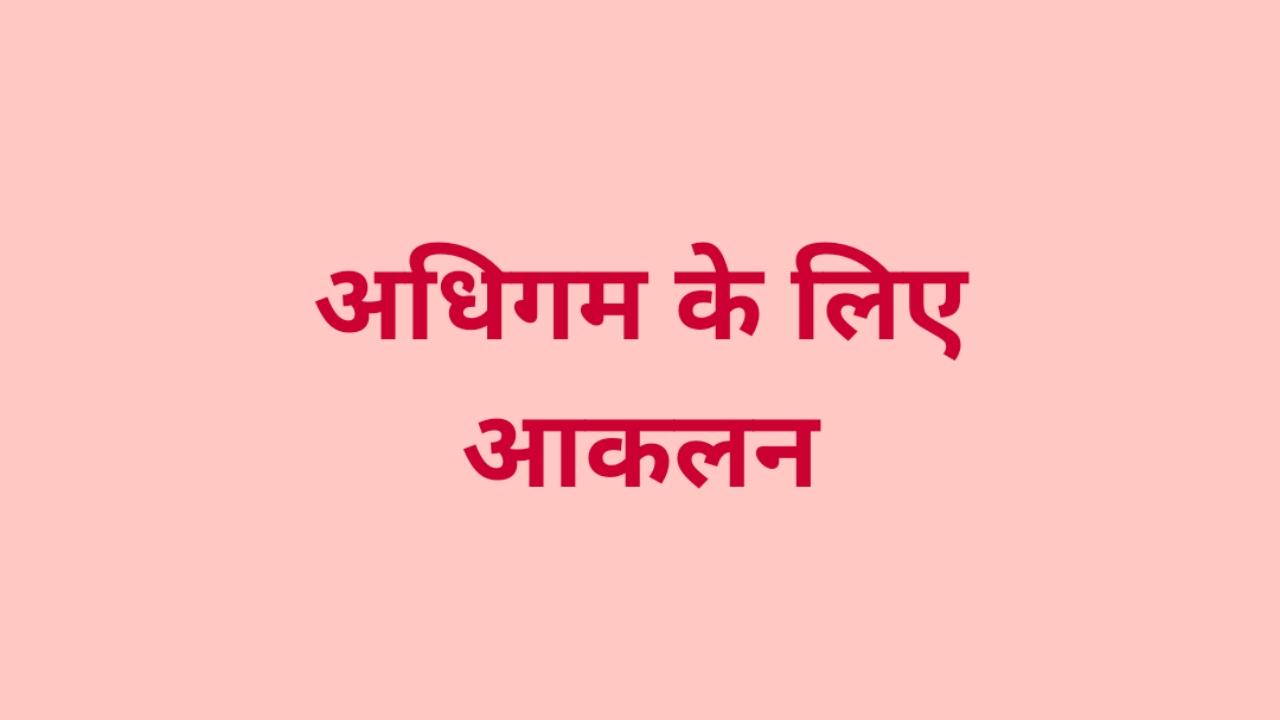
शिक्षा में मूल्यांकन की भूमिका (Role of Evaluation in Education)
शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का संकेत करता है कि शिक्ष्यमाण ने कौन-सा और कितना गुण या विशेषताएँ प्राप्त किया है उसका क्या मूल्य और उपयोगिता है। मूल्यांकन यह भी संकेत करता है कि अध्यापक द्वारा निश्चित किया गया शैक्षिक कार्यक्रम सफल हुआ है या नहीं और किस प्रकार से किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मूल्यांकन, छात्र और अध्यापक तथा समाज और संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता है। मूल्यांकन इस विचार से कुछ भूमिकायें पूरी करता है जिन्हें जाना आवश्यक जान पड़ता है। मूल्यांकन की भूमिकायें अग्रलिखित कही जा सकती हैं-
- मापन और मूल्य निर्धारण की भूमिका
इसका तात्पर्य यह है कि मूल्यांकन के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि किस छात्र में कौन-सा गुण किस रूप में और कितनी मात्रा में विद्यमान है। उदाहरण के लिए, किसी छात्र में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक आदि गुण कितना है इसकी जानकारी मूल्यांकन की विविध प्रविधियों से होती है। किस दिशा की ओर झुकाव अधिक अथवा कम है यह भी मूल्यांकन के द्वारा होता है।
- प्रगति और सुधार सम्बन्धी प्रवेश की भूमिका
मूल्यांकन की प्रविधियों के प्रयोग से हमें यह ज्ञात होता है कि छात्र की क्या प्रगति है। यदि प्रगति नहीं होती है तो उसमें सुधार करने के लिये प्रयत्न होता है। तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा छात्र को प्रगति करने की प्रेरणा भी मूल्यांकन की सहायता से दी जा सकती है। अतः भूमिका को प्राप्त करने के लिए राइटस्टोन के विचारानुसार मूल्यांकन को शिक्षा के प्रयोजन के अनुकूल होना चाहिए, मूल्यांकन का प्रोग्राम व्यापक होना चाहिए, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए और विभिन्न तरीकों से बहुत से साक्ष्यों को संग्रह करना चाहिए।
- निदानात्मक और पूर्व कथनात्मक भूमिका
विभिन्न प्रविधियो के प्रयोग से अध्यापक को छात्र के बारे में पर्याप्त जानकारी होती है। छात्र की अच्छाइयों और बुराइयों का ज्ञान होता है। और जो भी कमी और दोष छात्र में मिलते हैं उनके कारणों को मालूम करना मूल्यांकन की भूमिका होती है। इस प्रकार से मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में निदानात्मक भूमिका पूरी करता है। जो भी जानकारी छात्र के सम्बन्ध में उसकी योग्यता, क्षमता आदि के बारे में होती है। उसी के आधार पर उसके भविष्य को भी बताया जा सकता है। जहाँ मूल्यांकन की पूर्व कथनात्मक भूमिका पाय जाती है। इसके उदाहरण में यह कहा जा सकता है कि यदि कोई छात्र मूल्यांकन के फलस्वरूप गणित विषय में बहुत निम्न स्थान रखता है तो उसके निम्न स्थान रखने के कारणों को भी मूल्यांकन के द्वारा मालूम कर सकते हैं।
- उपचारात्मक भूमिका
मूल्यांकन के द्वारा निदान का ज्ञान होता है और उसके आधार पर उपचार को भी व्यवस्था की जाती है। उदाहरण के लिए, छात्रों की सफलता के कारणों को जानकर उन साधनों का प्रयोग किया जा सकता है जिससे वे शिक्षा में सफल हो सकें। इसके लिए विभिन्न मूल्यांकन प्रविधियों की सहायता ली जा सकती है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी हिन्दी भाषा में लगातार असफल होता है तो उसे किसी अन्य भाषा का परीक्षण देकर उसकी सफलता जानी जा सकती है। इसके बाद उसी भाषा में शिक्षा देकर छात्र की कमजोरी का उपचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हिन्दी भाषा के विभिन्न क्षेत्रों में भी कमजोरी मालूम होती है उसे भी दूर करने के लिए विभिन्न मूल्यांकन साधनों का प्रयोग करते हैं।
- मानक निर्धारण की भूमिका
समाज में जो संस्थाएं बनती है और उनके द्वारा जो क्रियाएँ होती है उनके लिए कुछ मानक निर्धारित होते हैं। इन मानकों का सम्बन्ध अध्यापक, शिक्षाविधि, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक विद्यालय व्यवस्था और अन्य शैक्षिक स्थितियों से होता है। मूल्यांकन की विभिन्न विधियों की सहायता से यह स्पष्ट हो जाता है कि अध्यापक का क्या स्तर है अथवा विद्यालय का स्थान क्या है या विद्यालय में छात्र अनुशासित है या नहीं। इससे यह बात मालूम होती है कि मूल्यांकन की भूमिका शिक्षा के विभिन्न प्रसंगों के लिये मानक निर्धारण की भी होती है।
- शिक्षा की दिशा निश्चित करने की भूमिका
मूल्यांकन का सम्बन्ध शिक्षा के उद्देश्य से भी होता है। मूल्यांकन के द्वारा यह ज्ञात होता है कि शिक्षा अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर है या नहीं है। यदि शिक्षा अपने उद्देश्य से दूर हो जाती है तो उसे उचित दिशा की ओर ले जाना आवश्यक होता है। यहाँ पर मूल्यांकन की भूमिका दिखायी देती है। उदाहरण के लिए, मूल्यांकन से ज्ञात हुआ है कि आज अपने देश में शिक्षा का स्तर नीचे गिर गया है तथा छात्र के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसीलिए शिक्षा की दिशा को कोठारी कमीशन ने 10+2+3 की व्यवस्था द्वारा बदलने की संस्तुति की है। परन्तु यह मूल्यांकन की ही भूमिका कही जा सकती है।
| मापदंड | आकलन | मूल्यांकन |
| 1. विषय वस्तु
2. केंद्र
3. उपयोगिता
4. मुख्य भूमिका 5. प्रतिपुष्टि का आधार
6. रिपोर्ट का उपयोगकर्ता
7. समय |
1. आकलन रचनात्मक तथा अधिगम की उन्नति के लिए होता है।
2. आकलन में प्रक्रिया उन्मुख होती है। 3. यह कमियों का निदान करता है। 4. विद्यार्थी और शिक्षक दोनों की भूमिका अहम होती है। 5. आकलन का आधार व्यापक है जो की निरीक्षण पर आधारित होता है। 6. विद्यार्थी (प्रदर्शन में सुधार के लिए) और शिक्षक (नैदानिक) शिक्षण दोनों के लिए है। 7. आकलन सतत् चलता है। |
1. मूल्यांकन योगात्मकता के माध्यम से विद्यार्थियों की संप्राप्ति को जाना जाता है।
2. मूल्यांकन उत्पाद उन्मुख होता है। 3. मूल्यांकन निर्णयात्मक होता है जिसमें ग्रेट अंक के रूप में देखा जाता है। 4. मूल्यांकन में सिर्फ शिक्षक की भूमिका होती है। 5. पूर्व निर्धारित मानक पर आधारित गुणवत्ता के स्तर के रूप में होता है। 6. मूल्यांकन के उपयोगकर्ता माता-पिता तथा अन्य लोग और संस्थाएं होती है। 7. मूल्यांकन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होता है। |
सीखने का आकलन‘ एवं ‘सीखने के लिए आकलन’ में विभेद
(1) सीखने का आकलन’ आकलन व मूल्यांकन के व्यवहारवादी तथा योगात्मक प्रकृति की ओर संकेत करता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी के अधिगम उपलब्धि का आकलन किया जाता है यानी विद्यार्थी क्या सीखता है तथा कितना सीखता है, विद्यार्थी द्वारा पूर्व निर्धारित अधिगम उद्देश्यों तथा अपेक्षित अधिगम परिणामों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है? इसका विद्यार्थी के अधिगम प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं होता। यह आकलन यह बताने में असमर्थ होता है कि विद्यार्थी कैसे सीखता है, उसके सीखने की शैली क्या है, वह अपने किस विशिष्ट क्षमता का उपयोग सीखने के लिए करता है।
(2) ‘सीखने का आकलन’ सम्पूर्ण अधिगम प्रक्रिया के पश्चात् पूर्व निर्धारित अधिगम उद्देश्य तथा अपेक्षित अधिगम परिणामों को ध्यान में रखकर विद्यार्थी के अधिगम निष्पत्ति का परीक्षण करती है। आकलन मुख्यतः लिखित या मौखिक परीक्षा द्वारा संचालित किया जाता है। परीक्षण में प्राप्त मात्रा या अंक विद्यार्थी के सीखने का द्योतक होती है। परीक्षण में दिए गए प्रश्नों के निश्चित तथा केवल एक उत्तर होते हैं जो शिक्षकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यदि विद्यार्थी इन प्रश्नों का सही उत्तर देता है या शिक्षकों के व्याख्यान तथा अनुदेशन के अनुरूप उत्तर देता है तो यह निर्णय लिया जाता है कि विद्यार्थी ने विषय-वस्तु या पाठ सम्पूर्ण रूप से अर्जित या सीख लिया है।
(3) ‘सीखने का आकलन’ विद्यार्थी के किसी विषय संबंधी अधिगम का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के समाप्त हो जाने के पश्चात् सत्रांत परीक्षा या कई इकाईयों के समाप्त हो जाने के पश्चात् तिमाही या छमाही लिखित या मौखिक परीक्षा के रूप में आकलन करती है।
(4) सीखने का आकलन मुख्यतः विद्यार्थी के अधिगम के संज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का आकलन करता है किंतु इसमें अधिगम के भावात्मक आयाम के आकलन की समुचित व्यवस्था नहीं होती। साथ ही साथ पाठ-सहगामी क्रियाओं के आकलन की भी उपेक्षा की जाती है।
(5) ‘सीखने का आकलन’ परंपरागत परीक्षा पद्धति को बढ़ावा देता है जिससे विद्यार्थियों में रटने की प्रवृति तथा आकलन व मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रति भय का भाव बना रहता है। इसमें शैक्षणिक गतिविधियों में गुणात्मक सुधार के लिए आवश्यक प्रतिपुष्टि का समुचित अवसर उपलब्ध नहीं होता।
(1) ‘सीखने के लिए आकलन’ आकलन व मूल्यांकन के निर्माणवादी तथा रचनात्मक एवं निदानात्मक प्रकृति की ओर संकेत करता है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी के अधिगम उपलब्धि के साथ-साथ उसके सीखने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह बताता है कि विद्यार्थी क्या सीखता है, कितना सीखता है तथा कैसे सीखता है? उसके सीखने का तरीका या शैली क्या है? सीखने की प्रक्रिया में वह किन विशिष्ट क्षमताओं तथा ज्ञान के स्रोतों को उपयोग में लाता है, उसके विचार तथा स्पष्टीकरण में कितनी नवीनता तथा मौलिकता है? इससे यह भी पता चलता है कि विद्यार्थी यदि सीख नहीं पाता तो क्यों सीख नहीं पाता, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में क्या सुधार लाया जाए, जिससे कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी सीख सके।
(2) ‘सीखने के लिए आकलन’ ऐसी आकलन व्यवस्था की ओर इंगित करता है जो वस्तुतः सीखने के लिए आयोजित की जाती है। यहाँ सीखने तथा आकलन की गतिविधियों के बीच सह-संबंध होता है यानी आकलन सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है
क्योंकि आकलन द्वारा प्राप्त तथ्य विद्यार्थियों के सीखने की युक्तियों तथा शैक्षणिक गतिविधियों में आवश्यक सुधार लाते हैं ताकी प्रत्येक विद्यार्थी प्रभावशाली ढंग से सीख सके।
(3) ‘सीखने के लिए आकलन प्रक्रिया में वैकल्पिक आकलन उपकरणों तथा युक्तियों का समुचित अवसर उपलब्ध होता है जिससे शिक्षकों को विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उनके रुचि तथा अभिक्षमता के अनुरूप विकल्प चयन करने का अवसर प्राप्त होता है ताकी उनके अधिगम का आकलन समुचित रूप से हो सके। सीखने के लिए आकलन विद्यार्थी के अधिगम तथा विकास का सतत रूप से आकलन करता है जिससे विद्यार्थियों के अधिगम में क्रमशः संवर्धन तथा विकास के लिए आवश्यक प्रतिपुष्टि नियमित रूप से प्राप्त होती है। साथ-ही-साथ इसमें में विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का आकलन भी सुनिश्चित होता है।
(4) ‘सीखने के लिए आकलन’ विद्यार्थियों का परीक्षा के प्रति भय के भाव को कम कर देता है क्योंकि उनके लिए उनके रुचि तथा अभिक्षमता के अनुरूप वैकल्पिक आकलन की व्यवस्था होती है तथा उनके विषय-संबंधी अधिगम का आकलन पाठ्यक्रम के छोटे-छोटे अंशों में किया जाता है। साथ ही साथ यह विद्यार्थियों में रटने की प्रवृति के स्थान पर विचारशील चिंतन क्षमता का विकास करता है।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के समुचित विकास का निरंतर और नियमित आकलन हैं जिसमें विकास के सभी पहलुओं का विभिन्न विधियों व उपकरणों द्वारा व्यापक आकलन किया जाता हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक विद्यार्थियों का ऐसा मूल्यांकन है जो सभी गतिविधियों की विकास का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उपयोग करके शिक्षक सभी प्रकार के मूल्यांकन गतिविधियों का उपयोग करके शिक्षार्थियों की कमियों का निदान कर सकता है।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की पृष्ठभूमि
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम को सबसे पहले CBSC के द्वारा कक्षा 9 के लिए लागू किया गया। इसकी महत्वता को देखते हुए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू किया गया।
सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता
वर्तमान मूल्यांकन व्यवस्था में किसी समय बिन्दु पर लिखित परीक्षा की व्यवस्था है, जब कि छात्र की संवृद्धि एवं विकास सम्पूर्ण सत्र में विकसित होता है। इसी प्रकार वर्तमान व्यवस्था में केवल शैक्षिक पहलुओं का मूल्यांकन होता है, जबकि छात्र के सर्वांगीण विकास में सह शैक्षिक पहलुओं का भी समान महत्व होता है।
यह अब सर्वमान्य तथ्य है कि प्रत्येक बच्चे की प्रकृति एवं सीखने के तरीके की गति में भिन्नता होती है तथा वे अलग-अलग तरीकों से सोखते हैं। हर विषय वस्तु को सीखने-सिखाने के तरीके में भिन्नता होने के कारण प्रत्येक बच्चे की प्रस्तुति एवं अभिव्यक्ति भी पृथक एवं विशिष्ट होती है। अतः यह आवश्यक है कि बच्चों का मूल्यांकन कागज कलम परीक्षा के अतिरिक्त अन्य विधाओं द्वारा भी किया जाये। अन्य विधाओं के प्रयोग से बच्चों की स्मृति क्षमता के स्थान पर अन्य उच्चतर क्षमताओं यथा-अभिव्यक्ति, विश्लेषण, समस्या का समाधान एवं अनुप्रयोग आदि दक्षताओं का विकास संभव होगा। चूँकि प्रत्येक बच्चे की प्रकृति विशिष्ट है और शिक्षण पद्धतियाँ भी भिन्न होती है, अतः एक समान मूल्यांकन पद्धति उपयुक्त नहीं हो सकती है। अतः सतत् व व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। सी.सी.ई. की आवश्यकता को निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा दर्शाया गया है –
(1) शिक्षार्थी के ज्ञान और पाठ्यक्रम के विषयों और अन्य विषयों के बारे में उसकी प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए विविध प्रकार के तरीकों का उपयोग करना।
(2) सूचना निरंतर एकत्र करते रहना और उसके अभिलेखबद्ध करना।
(3) प्रत्येक विद्यार्थी के प्रत्युत्तर देने और सीखने के तरीके और उसमें लगने वाले समय को महत्त्व देना।
(4) निरंतर आधार पर रिपोर्ट देना और प्रत्येक विद्यार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना।
(5) ‘फीडबैक’ मुहैया करना, जिससे सकारात्मक कार्यवाही की जा सकेगी और विद्यार्थी को बेहतर ढंग से कार्य करने में सहायता मिलेगी।
(6) बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना।
(7) मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाना।
(8) अध्यापक को सृजनात्मक अध्यापन के लिए गुंजाइश मुहैया करना।
(9) निदान और उपचार के साधन की व्यवस्था करना।
(10) अपेक्षाकृत अधिक कौशलों वाले शिक्षार्थियों का निर्माण करना।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएँ/महत्व
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चे के विकास के सभी पहलुओं का पता चलता हैं। इसके द्वारा शिक्षक को सीखने के दौरान छात्रों को होने वाली कठिनाइयों का पता चलता हैं। शिक्षक अनेक गतिविधियों एवं उपकरणों के माध्यम से यह पता करते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा एवं उन्हें सीखने में कहाँ मदद की आवश्यकता है। इस प्रकार वे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं।
(1) शिक्षा के सभी पहलुओं में छात्रों का मूल्यांकन और मार्गदर्शन करना।
(2) शिक्षण को प्रभावी बनाना।
(3) छात्र प्रगति का निरंतर मूल्यांकन करना।
(4) भविष्य के लिए शिक्षण अधिगम योजना बनाने में मदद करना।
(5) विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना।
(6) विद्यार्थियों को अधिक कौशल के साथ तैयार करना।
(7) अध्यापन और शिक्षा-प्राप्ति की प्रक्रिया को शिक्षार्थी केन्द्रित क्रियाकलाप बनाना।
(8) चिंतन की प्रक्रिया पर जोर देना और कंठस्थ करने पर बल न देना।
जैसा कि नाम से पता चलता है, मात्रात्मक टिप्पणियां संख्याओं के साथ सौदा करती हैं, क्योंकि वे व्यक्ति को परिणामों का ब्योरा देते हैं ये अवलोकन यंत्रों के साथ किया जा सकता है जो उपयोगकर्ता को विभिन्न भौतिक मात्राओं को जानने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, थर्मामीटर का उपयोग किसी ऑब्जेक्ट के तापमान को बताता है, शासक ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जानने में मदद कर सकता है, वजन संतुलन से शोधकर्ता वस्तुओं के वजन को जानने की अनुमति देता है, और बीकर तरल पदार्थ की मात्रा के बारे में जानने की अनुमति देता है । इसका मतलब है कि मात्रात्मक अवलोकन परिणाम दे सकते हैं जिन्हें मापा जा सकता है।
गुणात्मक अवलोकन में फोकस संख्याओं पर नहीं बल्कि गुणवत्ता पर है इस तरीके से इकट्ठा की गई जानकारी मात्रात्मक होने के लिए खुद को उधार नहीं देती है। जब अनुसंधान मानव व्यवहार के बारे में होता है, गुणात्मक अवलोकन जानकारी इकट्ठा करने का बहुत ही कुशल स्रोत है, बिना खुद को या व्यवहार के बारे में बताए विषयों के बिना, विश्लेषण के लिए डेटा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। जानवरों पर शोध के मामले में भी, गुणात्मक अवलोकन जानकारी प्राप्त करने का अधिक विश्वसनीय स्रोत है।
गुणात्मक और मात्रात्मक अवलोकन के बीच अंतर
अध्ययन के लक्ष्यों और अनुप्रयोगों से लेकर उनके साइकोमेट्रिक गुणों तक गुणात्मक और मात्रात्मक अवलोकन के बीच अंतर कई अलग-अलग पहलुओं में होता है। उनमें से प्रत्येक ने बदले में,, फायदे और नुकसान जो इसे कुछ परिस्थितियों में अधिक उपयुक्त बनाते हैं.
यद्यपि बहुत से लोग गुणात्मक तरीकों की उपयोगिता को कम आंकते हैं, जैसा कि हम देखेंगे, वे उन लोगों से भिन्न घटनाओं के विश्लेषण की अनुमति देते हैं जो समान तथ्यों को गहन परिप्रेक्ष्य से संबोधित करने की अनुमति देने के अलावा, मात्रात्मक तरीकों के हित का ध्यान केंद्रित करते हैं।.
- अध्ययन की वस्तु
मात्रात्मक अवलोकन के अध्ययन का उद्देश्य स्थिर डेटा है जिसमें से संभाव्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं. गुणात्मक तरीके मुख्य रूप से प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वह है, गतिशील पहलुओं में, और विश्लेषण के विषयों के परिप्रेक्ष्य से घटना के व्यक्तिपरक अनुभव पर ध्यान केंद्रित करें.
- उद्देश्य और अनुप्रयोग
गुणात्मक अवलोकन का मुख्य उद्देश्य एक घटना का प्रारंभिक अन्वेषण, विवरण और समझ है। इस अर्थ में, हम कह सकते हैं कि गुणात्मक तरीके विशिष्ट घटनाओं के आसपास परिकल्पना की पीढ़ी पर ध्यान केंद्रित करते हैं; कभी-कभी निष्कर्ष को इन अध्ययनों से प्रेरण के माध्यम से निकाला जा सकता है।
इसके विपरीत, मात्रात्मक अवलोकन का आमतौर पर वैज्ञानिक प्रक्रिया में बाद के बिंदु पर उपयोग किया जाता है: परिकल्पना का परीक्षण, अर्थात्, इसकी पुष्टि या खंडन में. इस प्रकार, उनके पास एक मुख्य रूप से कटौतीत्मक चरित्र है और कई मामलों में वे सिद्धांत के विश्लेषण और विशिष्ट समस्याओं के आसपास कार्रवाई के पाठ्यक्रमों की सिफारिश से जुड़े हैं।
- विश्लेषण बिंदु
चूंकि गुणात्मक शोध विशेष व्यक्तियों के दृष्टिकोण से घटना की खोज पर केंद्रित है, इसलिए इसमें अनिवार्य रूप से एक व्यक्तिपरक चरित्र है, हालांकि यह जरूरी नहीं कि पद्धतिगत कठोरता की कमी है। दूसरी ओर, मात्रात्मक अवलोकन, उन प्रभावों का विश्लेषण करने का प्रयास करती हैं, जिन्हें निष्पक्ष रूप से मापा जा सकता है.
हालांकि, और इसके विपरीत जो अक्सर बचाव किया जाता है, मात्रात्मक तरीके पूरी तरह से उद्देश्य नहीं हैं: वे शोधकर्ताओं की कार्रवाई पर विशेष रूप से निर्भर करते हैं, जो उन चरों का चयन करते हैं जो अध्ययन के उद्देश्य होंगे, विश्लेषण करते हैं और इनके परिणामों की व्याख्या करते हैं। इसलिए, वे स्पष्ट रूप से मानव त्रुटि के लिए अतिसंवेदनशील हैं.
- डेटा का प्रकार
मात्रात्मक अवलोकन के आंकड़े संख्यात्मक प्रकार के होते हैं; इस कारण से उन्हें प्रतिकृति के लिए एक निश्चित दृढ़ता और क्षमता प्रदान की जाती है जो डेटा से परे इनविटेशन बनाने की अनुमति देगा। गुणात्मक अवलोकन में प्राथमिकता को किसी विशेष तथ्य पर जानकारी की गहराई और समृद्धि के लिए दिया जाता है और निष्कर्ष इस तक सीमित हैं।
- कार्यप्रणाली
संख्यात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, मात्रात्मक तरीके वास्तविकता के कई ठोस पहलुओं के विशिष्ट और नियंत्रित माप की अनुमति देते हैं। इसके अलावा यह संभव बनाता है डेटा का उपयोग करके सांख्यिकीय विश्लेषण करना, जो बदले में सूचना के विभिन्न सेटों की तुलना और परिणामों के सामान्यीकरण के पक्ष में होगा.
इसके विपरीत, गुणात्मक अवलोकन मुख्य रूप से भाषा, विशेष रूप से कथा रिकॉर्ड के आधार पर डेटा का उपयोग करता है। विश्लेषण के तरीकों में बहुत अधिक प्रकृतिवादी चरित्र है और एक बड़ा महत्व संदर्भ और तत्वों के बीच संबंधों को दिया जाता है जो अध्ययन की घटना को बनाते हैं, और न केवल इन को अलग से.
- तकनीक का इस्तेमाल किया
गुणात्मक कार्यप्रणाली का उपयोग करने वाले अवलोकन इस तरह के तरीकों का उपयोग करते हैं गहराई से साक्षात्कार, प्रतिभागी अवलोकन या बहस और समूह वार्तालाप। इन तकनीकों में मात्रात्मक दृष्टिकोण की तुलना में कम संरचना स्तर है, जिसमें प्रश्नावली और व्यवस्थित अवलोकन रिकॉर्ड जैसी विधियां शामिल हैं।.
- विश्लेषण का स्तर
जबकि मात्रात्मक अवलोकन अध्ययन की वस्तुओं के विशिष्ट पहलुओं का विश्लेषण करता है, गुणात्मक अवलोकन में एक अधिक समग्र चरित्र होता है; इसका मतलब यह है कि यह तथ्यों की संरचना और तत्वों के बीच की गतिशीलता को समझने की कोशिश करता है जो उन्हें विशेष के बजाय वैश्विक तरीके से रचना करता है।
- सामान्यीकरण की डिग्री
सिद्धांत रूप में, मात्रात्मक तरीके निष्कर्ष निकालने और इस उच्च स्तर पर सामान्य बनाने के लिए एक बड़ी आबादी से प्रतिनिधि नमूनों का उपयोग करते हैं; इसके अलावा, वहाँ हैं तकनीकें जो त्रुटि की संभावना को मापने और कम करने की अनुमति देती हैं. परिणामों के सामान्यीकरण के लिए कठिनाई गुणात्मक का सबसे विशिष्ट दोष है.
- वैधता और विश्वसनीयता
मात्रात्मक अवलोकन की विश्वसनीयता और विश्वसनीयता मुख्य रूप से डेटा को मापने और विस्तृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों और उपकरणों पर निर्भर करती है। गुणात्मक कार्यप्रणाली के मामले में, ये गुण अवलोकन की क्षमता के साथ एक बड़ी हद तक संबंधित हैं, और अधिक व्यक्तिपरक चरित्र हो सकते हैं।
साक्षात्कार का अर्थ
हमारे जीवन और सामान्य व्यवहार में कई तरह के साक्षात्कार होते हैं, जैसे व्यस्त लोग, उच्च अधिकारियों से मिलना, नौकरी के लिए या संगठन में प्रवेश पाने के लिए आदि। ऐसे साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कृत की क्षमता का परीक्षण करता है, यानी साक्षात्कारकर्ता उसकी क्षमता की जांच करता है। लेकिन सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण में साक्षात्कारकर्ता न केवल साक्षात्कृत की क्षमता का परीक्षण करता है बल्कि अपने शोध से संबंधित आवश्यक तथ्यों का संकलन भी करता है।
वास्तव में ‘साक्षात्कार’ शब्द अंग्रेजी के ‘interview’ (इंटरव्यू) का हिंदी रूपांतर है, इसलिए यदि इंटरव्यू शब्द को समझें तो inter का अर्थ भीतर या अंदर होता है और interview का अर्थ होता है देखना। अर्थात साक्षात्कार का वास्तविक अर्थ देखना (अन्तरदर्शन) होता है।
दूसरे शब्दों में ‘interview’ का अर्थ है समागम । सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार विधि का प्रयोग सामग्री एवं सूचना एकत्र करने के लिए किया जाता है। साक्षात्कार विधि मनुष्य की इन्द्रियों पर आधारित है अर्थात् यह वार्तालाप द्वारा सूचना एवं सामग्री का संग्रह करती है। यदि हम एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और भावनाओं को जानना चाहते हैं तो उसके लिए संवाद सबसे उपयुक्त माध्यम है।
साक्षात्कार एक व्यवस्थित पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य से आमने-सामने संवाद, बातचीत और प्रतिक्रिया करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है जिसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता की भावनाओं, विचारों, दृष्टिकोणों और आंतरिक जीवन का अध्ययन करता है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया भी है।
साक्षात्कार की परिभाषा
साक्षात्कार के अर्थ को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए निम्नलिखित परिभाषाएँ देखने योग्य हैं-
पी. वी. यंग के अनुसार- “साक्षात्कार को एक क्रमबद्ध प्रणाली माना जा सकता है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति के आन्तरिक जीवन में अधिक या कम कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित है।”
सी. ए. मोजर के अनुसार- “एक सर्वेक्षण साक्षात्कार, सक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है, जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है।“
एफ. एन. करलिंगर के अनुसार- “साक्षात्कार एक आमने-सामने अंतर्वैयक्तित्क भूमिका वाली परिस्थिति है जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कारकर्ता, साक्षात्कार किये जाने वाले व्यक्ति, उत्तरदाता से, प्रश्न पूछता है। प्रश्नों का निर्माण शोध समस्या के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त उत्तरों की प्राप्ति हेतु किया जाता है।“
साक्षात्कार के प्रकार
साक्षात्कार के प्रकार निम्नलिखित हैं–
- व्यक्तिगत साक्षात्कार
इस प्रकार के साक्षात्कार मे केवल दो ही व्यक्ति होते हैं। एक साक्षात्कारकर्त्ता तथा दूसरा साक्षात्कारदाता। इसमे साक्षात्कारकर्त्ता प्रश्न पूछता जाता है तथा साक्षात्कारदाता प्रश्न का उत्तर देता जाता हैं।
- सामूहिक साक्षात्कार
इस प्रकार के साक्षात्कार मे दो या दो से अधिक साक्षात्कारकर्त्ता और अनेक साक्षात्कारदाताओं से समस्या से सम्बंधित सूचना एकत्रित करने का प्रयास करता है। कभी-कभी यह साक्षात्कार वाद-विवाद की सभा का रूप लेता है।
- औपरारिक साक्षात्कार
इस साक्षात्कार मे अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से मात्र औपचारिक संबंध स्थापित करके सिर्फ वे ही प्रश्न पूछता है, जो अनुसूची मे उल्लिखित रहते हैं। अनुसूची से बाहर वह किसी भी प्रकार के प्रश्न नही पूछता है। इसमें अनुसंधानकर्ता अनुसूची से नियंत्रण रहता है। उसको अनुसूची के प्रश्न, भाषा आदि के परिवर्तन मे किसी प्रकार की स्वतंत्रता नही रहती हैं।
- अनौपचारिक साक्षात्कार
यह साक्षात्कार मात्र अनौपचारिक से निर्वाह के लिए ही नही किया जाता हैं। इसमे अनुसन्धानकर्ता पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नही रहता हैं। वह अपनी इच्छा के अनुसार अनुसंधान के प्रश्नों के क्रमों मे संशोधन और परिवर्तन कर सकता हैं। इसके साथ ही वह सूचनादाताओं से नए प्रश्न पूछ सकता है।
- पुनरावृत्ति साक्षात्कार
इस प्रकार के साक्षात्कार मे अनुसंधानकर्ता एक से अधिक बार साक्षात्कार करके सूचनादाता से सूचना संकलित करता है। इसका प्रयोग परिवर्तन का अध्ययन करने तथा सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के प्रभाव जानने हेतु होता हैं।
- केन्द्रीय साक्षात्कार
इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग प्रायः किसी सामाजिक घटना, परिस्थितियों, फिल्म, रेडियो या दूरदर्शन कार्यक्रम का सूचनादाताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने हेतु किया जाता हैं।
- अनिर्देशित साक्षात्कार
यह अनौपचारिक, अनियन्त्रित तथा संचालित साक्षात्कार के समान होता हैं। इसमें साक्षात्कारकर्त्ता किसी पूर्व-निर्मित अनुसूची के अनुसार प्रश्न न करके अपनी इच्छा से प्रश्न करता है और साक्षात्कारदाता के समक्ष किसी समस्या को रख देता है। साक्षात्कारदाता जो विवरण, कहानी या वृत्तान्त प्रस्तुत करता है उसी के तथ्य संकलित होते हैं।
- अनुसंधान साक्षात्कार
इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य नवीन ज्ञान की खोज से संबंधित है। यह नवीन ज्ञान सामाजिक समस्याओं और सामाजिक घटनाओं से सम्बंधित होता है।
- कारक-परीक्षक साक्षात्कार
समाज मे विविध प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। इन घटनाओं के घटित होने के कुछ विशेष कारक या तत्व हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार मे इन्हीं कारकों की खोज की जाती है।
- प्रत्यक्ष साक्षात्कार
सामान्यतः साक्षात्कार प्रत्यक्ष ही होता है। इसे अनुसंधानकर्ता को काल्पनिक रूप से सूचनादाता के आन्तरिक जीवन मे प्रवेश के रूप मे देखा गया है।
- अप्रत्यक्ष साक्षात्कार
आमने-सामने न बैठकर अप्रत्यक्ष रूप से टेलीफोन या फिर किसी और माध्यम से साक्षात्कारकर्त्ता साक्षात्कारदाता से अध्ययन विषय से सम्बंधित तथ्यों के बारे मे वार्तालाप करके सूचना प्राप्त करना अप्रत्यक्ष साक्षात्कार कहलाता है।
- चयनात्मक साक्षात्कार
जब साक्षात्कार का प्रयोग किसी भी जीविका में नवीन नियुक्ति हेतु चयन के लिए किया जाता है तो इस प्रकार के साक्षात्कार को चयनात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कार प्रदाता से उस जीविका में उपयुक्तता से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षात्कारकर्ता कुछ ऐसे प्रश्न पूछता है जिसके आधार पर साक्षात्कार प्रदाता की अभिवृत्ति, अभिक्षमता, योग्यताओं, आचरण आदि के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। इस तरह के साक्षात्कार का मूल उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि साक्षात्कार प्रदाता कहां तक अपनी अभिवृत्ति, अभिक्षमता, योग्यताओं के आधार पर अमुक नौकरी के लिये योग्य होगा।
- शोध साक्षात्कार
इस प्रकार के साक्षात्कार में किसी विषय पर विभिन्न व्यक्तियों के विचारों को जानने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति की रूचि उन तथ्यों में होती है जो कि साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति की रूचि उन तथ्यों में होती है जो कि साक्षात्कार देने वाले के विचारों में सम्मिलित है। इसके लिए कुछ ही प्रतिनिधि व्यक्तियों को छांटकर केवल उन्हीं का साक्षात्कार किया जाता है। इन प्रतिनिधि व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पूर्ण जनसंख्या के विचारों के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इसलिए इसे न्यादर्श साक्षात्कार भी कहा जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य शोध समस्याओं के प्रस्तावित समाधान के बारे में एक विस्तृत ब्यौरा तैयार करना होता है। इस तरह का शोध अधिकतर उन वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है जो किसी विशेष समस्या का उत्तर तुरन्त पा लेना चाहते है।
- निदानात्मक साक्षात्कार
इस प्रकार के साक्षात्कार के माध्यम से साक्षात्कारकर्ता बालक या किसी व्यक्ति की समस्या के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। किसी विद्यालय में शिक्षक द्वारा छात्रों के किसी विशेष समस्या के विषय में सूचनाएं एकत्र करने के लिये प्रयुक्त साक्षात्कार इस प्रकार के साक्षात्कार का उदाहरण है।
- उपचारात्मक साक्षात्कार
निदानात्मक साक्षात्कार के बाद जब किसी छात्र की समस्या तथा उसके विषय में सूचनाएं एकत्र कर ली जाती हैं तो उपचारात्मक साक्षात्कार में व्यक्ति से इस प्रकार का वार्तालाप किया जाता है कि उसको अपनी चिन्ताओं तथा समस्याओं से मुक्त किया जा सके तथा समायोजन सही तरीके से हो सके।
- तथ्य संकलन साक्षात्कार
इस साक्षात्कार में व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय से मिलकर तथ्य संकलित किए जाते हैं। शिक्षक इसी साक्षात्कार द्वारा छात्रों के सम्बन्ध में तथ्य एकत्रित करते हैं। इसके तीन प्रमुख उद्देश्य हैं
(क) अन्य विधियों द्वारा संग्रहीत किये गये तथ्यों में अपूर्णताओं न्यूनताओं या कमियों को पूर्ति करना। कुछ तथ्य अन्य विधियों द्वारा प्राप्त नहीं हो पाते हैं। साक्षात्कार में उन सूचनाओं को एकत्रित करने का प्रयत्न किया जाता है जो मनोवैज्ञानिक जांचों द्वारा प्राप्त नहीं हो पाती है।
(ख) पहले से संकलित की गयी सूचनाओं की पुष्टि करने के लिए तथ्य संकलन साक्षात्कार किया जाता है।
(ग) तथ्य संकलन साक्षात्कार का तीसरा उद्देश्य शारीरिक रूप से अवलोकन करना है। बहुत से छात्रों में अनेक शारीरिक दोष पाये जाते हैं जिनका ज्ञान मनोवैज्ञानिक जांचों से नहीं हो सकता है। इसके साथ ही साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति का बातचीत करने तथा आचरण करने के ढंग का ज्ञान होता है।
साक्षात्कार के उद्देश्य
साक्षात्कार केवल दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप करने की प्रक्रिया नहीं है, अपितु इसके अनेक उद्देश्य होते हैं, अर्थात् साक्षात्कार लेने वाले और साक्षात्कारदाता के बीच होने वाली बातचीत एक विशेष उद्देश्य के लिए होती है। साक्षात्कार के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
(1) प्रत्यक्ष संपर्क
साक्षात्कार का पहला उद्देश्य सूचनादाताओं से सीधे या आमने-सामने संपर्क स्थापित करके उनसे डेटा संकलित करने में शोधकर्ता की सहायता करना है। आमने-सामने बैठकर शोधकर्ता न केवल सूचनादाताओं से खुलकर बातचीत करता है बल्कि उनके चेहरे के भावों को भी समझने की कोशिश करता है।
(2) अवलोकन का अवसर
साक्षात्कार सूचनादाताओं के आंतरिक और बाह्य जीवन दोनों का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है। शोधकर्ता के पास सूचनादाताओं के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर भी होता है।
(3) व्यक्तिगत सूचनाओं का संग्रह
साक्षात्कार का उद्देश्य सूचनादाताओं के आंतरिक जीवन पर विचार करना है। पी.वी. यंग के अनुसार इसका उद्देश्य सूचनादाता के व्यक्तित्व का चित्र बनाना है। इसलिए, यह सूचनादाताओं के आंतरिक जीवन से संबंधित आंकड़े एकत्र करने में विशेष रूप से सहायक तरीका है, जिसे हम अवलोकन के माध्यम से नहीं देख सकते हैं।
(4) परिकल्पनाओं का निर्माण
साक्षात्कार परिकल्पना निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका उपयोग दो या दो से अधिक चरों के अंतर्संबंधों को जानकर यानी खोजपूर्ण तरीके से जानकारी प्राप्त करके परिकल्पना बनाने के लिए किया जाता है।
(5) अन्य प्रविधियों को प्रभावपूर्ण बनाना
जबकि साक्षात्कार अपने आप में एक पूर्ण विधि है, इसे अन्य विधियों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए एक पूरक विधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यह अनुसूची और अवलोकन में एक पूरक विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। पी. वी. यंग के अनुसार, “साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान में एक अलग उपकरण नहीं है, बल्कि यह अन्य विधियों और प्रविधियों का पूरक है। यह अध्ययन को गहन बनाता है और अन्य स्रोतों और साधनों द्वारा एकत्रित सूचनाओं को नियंत्रित करता है।”
साक्षात्कार की समस्याएं
विश्वसनीय और प्रमाणित डेटा का संग्रह सामाजिक शोध में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कई तरीकों से किया जाता है। साक्षात्कार के माध्यम से विश्वसनीय एवं प्रमाणिक आँकड़ों का संकलन करना एक कठिन कार्य है क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ त्रुटियाँ रह जाती हैं जिन्हें हम साक्षात्कार समस्याएँ कह सकते हैं। इन त्रुटियों को चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है –
- साक्षात्कारकर्ता से संबंधित त्रुटियाँ
साक्षात्कारकर्ता की कुछ व्यक्तिगत विशेषताएँ साक्षात्कार द्वारा एकत्रित किए गए आँकड़ों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को प्रभावित करती हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं:
* साक्षात्कारकर्ता का व्यक्तित्व,
* साक्षात्कारकर्ता का अनुभव,
* साक्षात्कारकर्ता की आयु, लिंग और शिक्षा,
* साक्षात्कारकर्ता की जाति, धर्म और सामाजिक वर्ग,
* साक्षात्कारकर्ता का रवैया और विचारधारा और
* साक्षात्कारकर्ता की व्यक्तिगत आशाएँ और आकांक्षाएँ।
(2) साक्षात्कार उपकरण से संबंधित त्रुटियाँ
साक्षात्कार उपकरण में त्रुटियां डेटा की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को भी प्रभावित कर सकती हैं। साक्षात्कार उपकरण की प्रमुख त्रुटियां इस प्रकार हैं:
* प्रश्नों की जटिल संरचना,
* प्रश्नों के उचित क्रम का अभाव,
* साक्षात्कार अनुसूची की अत्यधिक लंबाई,
* प्रश्नों का अस्पष्ट और दोषपूर्ण सूत्रीकरण और
* भावनात्मक या उत्तेजक प्रश्नों की अनुसूची।
(3) साक्षात्कार संचालन से संबंधित त्रुटियां
यदि साक्षात्कार की मुख्य प्रक्रिया ठीक प्रकार से संचालित नहीं की जाती है तो भी आंकड़ों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता प्रभावित होती है। इसमें हम निम्नलिखित त्रुटियों को शामिल कर सकते हैं-
* सवाल ठीक प्रकार से न पूछना,
* संकेतन से सम्बन्धित अन्तर,
* साक्षात्कार के लिए अनुपयुक्त स्थान का चयन,
* साक्षात्कार के लिए अनुपयुक्त समय का चयन,
* सूचनादाता के साथ उचित संचार का अभाव, और
* अपने दृष्टिकोण के अनुरूप प्रतिक्रियाओं को घुमाना या फिर से लिखना।
(4) उत्तरदाताओं से संबंधित त्रुटियां
कई बार, उत्तरदाताओं के साथ ठीक से संवाद नहीं कर पाने के कारण, कई त्रुटियां डेटा की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को प्रभावित करती हैं। उत्तरदाताओं से संबंधित प्रमुख त्रुटियाँ इस प्रकार हैं:
* उत्तरदाताओं की स्थिति,
* उत्तरदाताओं की दोषपूर्ण स्मृति,
* उत्तरदाताओं की इच्छा सही उत्तर न देने की,
* उत्तरदाताओं के व्यक्तिगत दृष्टिकोण और विचारधारा,
* उत्तरदाताओं के मन में प्रश्नों के बारे में संदेह और
* अनुसंधान समस्या के प्रति उत्तरदाताओं की उदासीनता।
साक्षात्कार के गुण
सामाजिक अनुसंधान में यदि हम साक्षात्कार को सूचना एकत्र करने की एक विधि के रूप में मूल्यांकित करें तो अन्य विधियों की भाँति इसके भी कुछ गुण और कुछ दोष हैं। चूंकि साक्षात्कार सूचक के साथ सीधे संपर्क का अवसर प्रदान करता है, यह बाहरी व्यवहार और आंतरिक विचारों और दृष्टिकोण दोनों का अध्ययन करने में एक बहुत ही उपयोगी तरीका है। इसके मुख्य गुणों की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है:
(1) विस्तृत सूचनाओं की प्राप्ति
साक्षात्कार सभी प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करने की एक बहुत ही सरल विधि है। इसके माध्यम से सभी प्रकार के सूचनादाताओं से जानकारी एकत्र की जा सकती है, चाहे वे पढ़े-लिखे हों या अशिक्षित या किसी भी वर्ग के हों।
(2) अमूर्त परिघटनाओं का अध्ययन
अमूर्त घटनाओं और अनदेखी तथ्यों का साक्षात्कार क्योंकि यह किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति के अध्ययन में मदद करता है। इन घटनाओं एवं अदृश्य तथ्यों का ज्ञान संबंधित एवं प्रभावित व्यक्तियों से साक्षात्कार कर उनसे जानकारी प्राप्त कर प्राप्त किया जा सकता है।
(3) पिछली घटनाओं का अध्ययन
साक्षात्कार पूर्व में घटी घटनाओं का वास्तविक परिचय भी देता है। पूर्व में हुई किसी घटना से प्रभावित सूचनादाता उस घटना का वर्णन कर सकता है और शोधकर्ता को सटीक जानकारी दे सकता है। यदि किसी विशेष घटना से प्रभावित व्यक्ति उस घटना के बारे में नहीं बताता है तो ऐसी घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता है।
(4) सामाजिक-मनोवैज्ञानिक अध्ययन में सहायक
साक्षात्कार विशेष रूप से व्यक्ति के सामाजिक-मनोवैज्ञानिक अध्ययन में एक बहुत ही उपयोगी विधि है। इसके माध्यम से सूचनादाताओं की भावनाओं में उतार-चढ़ाव, उनकी धारणाओं और दृष्टिकोणों और आंतरिक विचारों और आवेगों का अध्ययन किया जा सकता है। चूंकि शोधकर्ता सूचनादाता के जीवन में प्रवेश करता है, जो उसके लिए अपेक्षाकृत पराया है, काल्पनिक रूप से, यह उसकी आंतरिक स्थिति को समझने में बहुत उपयोगी है।
(5) अन्तःप्रेरणा की सुविधा
चूंकि साक्षात्कार साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता के बीच आमने-सामने की मुलाकात है, इसलिए दोनों एक-दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। अन्तःप्रेरणा के कारण साक्षात्कारदाता साक्षात्कार द्वारा जो सूचना देता है वह किसी भी विधि से उपलब्ध नहीं हो सकती।
(6) लचीलापन
साक्षात्कार की विधि विषय-वस्तु और उसका संचालन दोनों ही बहुत लचीले होते हैं, जिसके कारण कई बार वह कई ऐसे तथ्य भी प्रकट कर देता है जिनका शोधकर्ता अनुमान भी नहीं लगा सकता।
(7) सूचनाओं की जाँच
साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त जानकारी को भी आसानी से जांचा जा सकता है। एक कुशल साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार के समय सूचनादाता के चेहरे पर भावनाओं और कई अन्य चीजों का मूल्यांकन करता है। साथ ही, यदि वह कुछ अस्पष्ट कहता है, तो शोधकर्ता उसे तुरंत स्पष्ट कर सकता है।
(8) सवालों को अच्छे से समझने का अवसर
साक्षात्कार में अनुसन्धानकर्ता का सूचनादाता से सीधा सम्पर्क होता है, जिससे सूचनादाता प्रश्नों को अच्छी तरह समझ सकता है। यदि उसे प्रश्नों को समझने में कोई कठिनाई हो रही है, तो वह साक्षात्कारकर्ता से उन्हें समझाता है।
(9) उत्तर न मिलने की संभावना समाप्त
चूंकि साक्षात्कार सूचनादाता के साथ सीधे और आमने-सामने संपर्क स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है, यह प्रतिक्रिया न मिलने की संभावना को समाप्त कर देता है। सीधे संपर्क के परिणामस्वरूप गैर-प्रतिक्रिया संबंधी समस्याएं हल हो जाती हैं।
साक्षात्कार के दोष
यद्यपि साक्षात्कार सभी प्रकार के सूचनादाताओं से सूचनाएँ एकत्रित करने की सर्वोत्तम विधि है, तथापि यह सुस्पष्ट नहीं है। इसमें पाए जाने वाले मुख्य दोष इस प्रकार हैं:
(1) अधिक खर्चीली
साक्षात्कार में, शोधकर्ता को समय और स्थान निर्धारित करने और फिर साक्षात्कार आयोजित करने के लिए प्रत्येक सूचनादाता के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना होता है। इसलिए, यह विधि अन्य विधियों की तुलना में अधिक महंगी है। यदि सूचनादाता अधिक व्यापक क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो उनसे संपर्क करना और भी कठिन और महंगा हो सकता है।
(2) मूल्यों में भिन्नता
यदि शोधकर्ता और सूचना देने वाले (जैसा कि ज्यादातर होता है) की सामाजिक पृष्ठभूमि में काफी अंतर है, दोनों के पास घटना के बारे में अलग-अलग विचार हैं, तो साक्षात्कार द्वारा प्राप्त जानकारी की स्वाभाविकता और विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।
(3) अनावश्यक सूचनाएं
साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं में बहुत सी बातें अनावश्यक होती हैं क्योंकि सूचनादाता बहुत सी बातों को बढ़ा-चढ़ा कर बताता है और बहुत सी अप्रासंगिक बातें बता देता है। सूचनादाता पर आश्रित होने के कारण कभी-कभी अनुसन्धानकर्ता को अनावश्यक बातें भी सुननी पड़ती है।
(4) याददाश्त पर निर्भरता
साक्षात्कार के समय साक्षात्कार में जानकारी लिखना सामान्यतः संभव नहीं होता, अतः साक्षात्कार के बाद प्राप्त सूचना को लिखने में स्मृति दोष के कारण कई महत्वपूर्ण तथ्यों के छूट जाने की सम्भावना रहती है। यदि किसी भूतकाल की घटना का अध्ययन किया जा रहा है तो यह आवश्यक नहीं है कि उस घटना से प्रभावित व्यक्ति ही उसका विवरण दे सकें।
(5) हीनता की भावना
अधिकांश साक्षात्कारों में, सूचना देने वाला शोधकर्ता के व्यक्तित्व और समस्या के बारे में उसके ज्ञान से इतना प्रभावित होता है कि वह हीन महसूस करता है, जिसके कारण वह जानकारी को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है ताकि उसकी हीन भावना प्रकट न हो। इससे सूचना की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
(6) व्यक्तिगत पक्षपात
साक्षात्कार में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने या पूर्वाग्रह की संभावना अधिक होती है क्योंकि केवल शोधकर्ता ही सूचनार्थी द्वारा दी गई जानकारी को जानता है और यदि वह चाहे तो प्राप्त जानकारी और डेटा को अपने दृष्टिकोण के अनुसार प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही, यदि सूचनादाता की मनोदशा अनुसंधानकर्ता को प्रभावित करती है, तो वह उसके द्वारा दी गई सूचना को अपने पक्ष में विकृत कर सकता है।
असाइनमेंट का अर्थ
असाइनमेंट- इस शब्द का उपयोग शिक्षा उद्योग में शिक्षकों द्वारा आवंटित किसी शैक्षणिक भाग या कार्य को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यह सीखने, अभ्यास करने और प्राप्त शिक्षण लक्ष्यों को प्रदर्शित करने का दायरा या अवसर प्रदान करता है। जब शिक्षक छात्रों को असाइनमेंट देते हैं, तो यह उन्हें इस बात का अवलोकन प्रदान करता है कि छात्रों ने पाठ से क्या समझा है। उन्हें यह भी पता चलता है कि क्या छात्रों को सीखे गए विषय पर स्पष्टता है और यदि नहीं, तो उन्हें किस बात पर संदेह है।
असाइनमेंट शिक्षकों के लिए सबसे आम मूल्यांकन विधियों में से एक है। शिक्षण विशेषज्ञों के एक भाग के रूप में, टीम ट्यूटरबिन जानती है कि छात्र विभिन्न प्रश्नों के साथ आते हैं जैसे- असाइनमेंट का अर्थ क्या है? यहां हम उन सभी का जवाब देंगे. आइए अर्थ से शुरू करते हैं। असाइनमेंट छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा है। असाइनमेंट न केवल छात्रों के लिए महत्व रखता है बल्कि शिक्षकों के लिए भी अत्यधिक महत्व रखता है। इससे उन्हें यह मापने में मदद मिलती है कि छात्रों ने अपने पाठों से कितना सीखा है और क्या उन्होंने शिक्षकों द्वारा उनके लिए निर्धारित सीखने के लक्ष्यों को हासिल किया है।
असाइनमेंट के प्रकार (Types of Assignment)
गृहकार्य अग्रलिखित आगरा प्रकार का हो सकता है–
(1) समस्या मूलक असाइनमेंट
इस प्रकार के गृहकार्य में विद्यार्थियों को उनकी पुस्तक या जीवन से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान दिया जाता है।
(2) अभ्यास असाइनमेंट
इस प्रकार के गृह कार्य में विद्यार्थियों को उनका पूर्वज्ञान का अभ्यास सिखाया जाता है।
(3) इकाई असाइनमेंट (Unit Assignment)
यह ऐसा असाइनमेंट होता है जिसमें विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली क्रियाओं में लगा दिया जाता है।
(4) सूचना एकत्रित करने वाले (Informatic)
इन असाइनमेंट में विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की सूचनायें एकत्रित करता है।
(5) स्मृति सम्बन्धी (Memorization Type)
इस कार्य में विद्यार्थी पढ़े हुये पाठ को मौखिक रूप से रटने का प्रयास करते हैं।
(6) अध्ययन सम्बन्धी (Study Type)
यह असाइनमेंट अत्यन्त सरल होता है। इसमें विद्यार्थियों को किसी विषय पर टिप्पणी तैयार करने के लिये कहा जाता है।
असाइनमेंट के लाभ
(1) विद्यार्थी का ज्ञानकोष बढ़ाएँ
विभिन्न विषयों के अलग-अलग विषयों पर असाइनमेंट दिए जाते हैं। कार्य के माध्यम से, छात्र अपनी समझ और ज्ञान के अनुप्रयोग पर विचार करते हैं। असाइनमेंट के माध्यम से छात्रों को मिलने वाले शीर्ष लाभों में से एक विभिन्न विषयों के बारे में उनके ज्ञान का विस्तार करना है। इसके अलावा, वित्त होमवर्क सहायता से , वे विविध विषयों पर अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और विषय में आसानी से महारत हासिल कर लेते हैं।
(2) अपना व्यावहारिक कौशल बढ़ाएँ
अगला लाभ जो बड़े पैमाने पर फायदेमंद साबित हुआ है वह असाइनमेंट के माध्यम से विकसित व्यावहारिक कौशल में वृद्धि है। असाइनमेंट करते समय, छात्र तार्किक और विश्लेषणात्मक कौशल, तर्क क्षमता और रचनात्मकता का निर्माण करते हैं। ये कौशल छात्रों को उनके शैक्षणिक जीवन में बेहतर प्रदर्शन करने और उनके आगामी व्यावसायिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए सशक्त बनाते हैं।
(3) अनुसंधान क्षमता बढ़ती है
होमवर्क का अभ्यास करने और असाइनमेंट करने से छात्रों को एक और उत्कृष्ट लाभ प्राप्त होता है, वह है उनकी बढ़ी हुई शोध क्षमता। विभिन्न विषयों पर गहन शोध के कारण, छात्रों को उपयोगी जानकारी खोजने और उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्रमबद्ध करने की क्षमता मिलती है। यह आदत उनकी शिक्षा के लिए सहायक बनती है और उनके पेशेवर जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है।
(4) अपने सीखने का दायरा बढ़ाएँ
यदि छात्रों पर बोझ न पड़े तो असाइनमेंट और होमवर्क सहायक होते हैं। यह सीखने को भी सुदृढ़ करता है और ज्ञान प्रतिधारण पर बड़ा प्रभाव डालता है। शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि ऐसे कार्य छात्रों को अपने पाठों को याद करने में सक्षम बनाते हैं जो उनके दिमाग में विषयों या विषय अवधारणाओं को ताज़ा रखते हैं। दूसरे शब्दों में, होमवर्क छात्रों के सीखने के दायरे को बढ़ाता है जो उन्हें अपने विषयों का पता लगाने और अध्ययन में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करता है।
(5) शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार
छात्रों पर किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 75% छात्रों ने स्वीकार किया है कि असाइनमेंट करने से उन्हें उच्च अंक प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने खुलासा किया कि छात्रों ने न केवल एक विषय के लिए अच्छा स्कोर किया, बल्कि लगातार असाइनमेंट के साथ उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन में काफी वृद्धि हुई।
(6) योजना एवं आयोजन कौशल को सशक्त बनाना
किसी कार्य को करने के लिए गहन योजना की आवश्यकता होती है। जानकारी की खोज, प्रासंगिक डेटा को छांटना और उसका उपयोग करना छात्रों के संगठन कौशल को बढ़ाता है। इसके बाद वे यह रूपरेखा बना सकेंगे कि उन्हें अपना काम कब और कैसे करना है। असाइनमेंट का प्रयास करने से उन्हें अपनी सीखने की आदतों को प्रबंधित करने और अपने शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अपने ज्ञान का बुद्धिमानी से उपयोग करने में सक्षम बनाया गया।
सांख्यिकी का अर्थ
सांख्यिकी का प्रयोग किसी भी विषय के वैज्ञानिक अध्ययन तथा विश्वसनीय आँकड़े प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सांख्यिकी डेटा के त्वरित और गहन विश्लेषण को सक्षम बनाती है।
सांख्यिकी के व्यापक प्रयोग के कारण आधुनिक युग को सांख्यिकी का युग कहा जाता है। जो भी तथ्य हों – प्राकृतिक, आर्थिक या सामाजिक – सभी को सांख्यिकीय भाषा में मापा, प्रस्तुत और व्याख्या किया जा सकता है। ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यिकी का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। आज अगर आप किसी तथ्य को अंकों से नहीं बता सकते हैं तो उसकी सत्यता पर संदेह रहेगा। यह भी कहा जाता है, “जो कुछ आप कह रहे हैं, यदि उसे संख्या में माप सकते हैं और व्यक्त कर सकते हैं, तब तो आप कुछ जानते है अन्यथा आपका ज्ञान अल्प एवं असंतोषजनक है।“ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्वपूर्ण स्थान है।
सांख्यिकी का महत्व
आज सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन एवं शोध कार्य में सांख्यिकी का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे-जैसे इसका उपयोग मानव ज्ञान, सामाजिक, भौतिक, जैविक, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और प्रशासन आदि हर क्षेत्र में किया जा रहा है, वैसे-वैसे इन विषयों में सांख्यिकी का उपयोग बढ़ता जा रहा है। सांख्यिकी वैज्ञानिक अनुसंधान में कई कार्य करती है। सामाजिक विज्ञानों में सांख्यिकी की आवश्यकता और महत्व इस प्रकार है:
(1) प्रदत्तों के वर्णन में
किसी समस्या के अध्ययन से प्राप्त प्रदन्त या आँकड़े । उन आंकड़ों का वर्णन करने में कई सांख्यिकीय विधियां उपयोगी होती हैं। उदाहरण के लिए, प्रदन्तों के आवृत्ति वितरण को बनाने, उन्हें विभिन्न प्रकार के रेखाचित्रों के साथ प्रदर्शित करने में सांख्यिकी का बहुत महत्व है। माध्य, माध्यिका और बहुलांक जैसे केंद्रीय रुझानों को मापने के तरीकों की मदद से सांख्यिकी प्रदत्तों या आँकड़ों का वर्णन करने में भी उपयोगी है।
आँकड़ों को स्पष्ट और आकर्षक तरीके से प्रदर्शित करने के लिए स्तम्भ रेखाचित्र, वृत्तचित्र, स्तम्भाकृति, आवृत्ति बहुभुज, सरल आवृत्ति बहुभुज, संचयी बारंबारता वक्र आदि विधियों का भी उपयोग किया जाता है। वर्णनात्मक सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके यह भी जाना जा सकता है कि अध्ययन या अनुसंधान से प्राप्त आंकड़ों की प्रकृति वितरित प्रकार की है या नहीं और क्या आंकड़ों की प्रकृति वितरण या वितरण के रूप में है।
(2) प्रदत्तों के सहसम्बन्ध के वर्णन में
कभी-कभी शोधकर्ता दो या अधिक प्रकार के आँकड़ों या दो या दो से अधिक समूहों के आँकड़ों के बीच सहसंबंध का अध्ययन करना चाहता है, या यह पता लगाना चाहता है कि दो या दो से अधिक समूहों के ये आँकड़ों एक दूसरे से किस हद तक सहसंबद्ध हैं। इन सवालों के जवाब के लिए, शोधकर्ता सांख्यिकी के सहसंबंध के तरीकों का उपयोग करता है।
(3) प्रतिगमन और भविष्यकथन
प्रतिगमन दो चरों के बीच का अनुपात है जो उनके संबंधित मध्यमान से घटता है। प्रतिगमन दो चरों की प्रकृति का ज्ञान भी प्रदान करता है। जब कोई शोधकर्ता किसी घटना या चर से संबंधित ज्ञान के आधार पर किसी घटना या चर का पूर्वानुमान या भविष्यकथन लगाना चाहता है, तो वह प्रतिगमन और सांख्यिकी की भविष्यवाणी से संबंधित विधियों का उपयोग करता है।
(4) वैज्ञानिक परिकल्पनाओं के परीक्षण में
वैज्ञानिकों द्वारा परिकल्पनाओं के परीक्षण में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। सवालों के जवाब पाने के लिए उसे टी-परीक्षण, सी.आर. परीक्षण, सैण्डलर का ए-परीक्षण, प्रसरण विश्लेषण, काई-वर्ग परीक्षण, मध्यांक परीक्षण और चिन्ह-परीक्षण आदि सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करता है।
(5) प्रतिदर्श चयन में
बड़ी संख्या में आबादी या जनसंख्या पर अपनी शोध समस्या के अध्ययन के दौरान, शोधकर्ता पूरी आबादी का अध्ययन करने के बजाय पूरी आबादी से कुछ अध्ययन इकाइयों का चयन करता है। इन चयनित अध्ययन इकाइयों को प्रतिदर्श कहा जाता है। अध्ययन समस्या की प्रकृति के अनुसार, शोधकर्ता सांख्यिकीय विधियों की सहायता से एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श का चयन करता है। इसके अलावा वह सांख्यिकीय विधियों की सहायता से प्रतिदर्श के आकार की गणना भी करता है।
(6) शैक्षणिक और शोध कार्य में
लगभग सभी देशों में शिक्षा, पाठ्यचर्या, शिक्षण और मूल्यांकन विधियों के उद्देश्यों में परिवर्तन की माँग को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षिक परीक्षण और शोध कार्य किए जाते हैं। सांख्यिकी इन कार्यों और परीक्षणों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की जाँच की जाती है। इससे न केवल त्रुटियों का ज्ञान होता है, बल्कि उनकी उपयोगिता का भी अनुमान लग जाता है।
(7) साहचर्य के आधार पर कारण-कार्य सम्बन्ध में
जब एक शोधकर्ता स्वतंत्र चर पर परतन्त्र चर के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है या कारण-प्रभाव संबंध का अध्ययन करना चाहता है, तो वह सांख्यिकीय विधियों की सहायता लेता है। उदाहरण के लिए, शिक्षा और आय के बीच संबंध खोजने के लिए, शोधकर्ता को न केवल समूहों के बीच सार्थकता की सार्थकता की जांच करनी होती है, बल्कि सहसंबंध की गणना भी करनी होती है।
(8) मापन और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में
मनोवैज्ञानिक मापन और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के निर्माण में सांख्यिकी विधियाँ बहुत अधिक उपयोगी हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के निर्माण में पदों का चयन करते समय परीक्षण बन जाने के बाद, परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता की गणना करने में सांख्यिकीय विधियाँ बहुत उपयोगी होती हैं। सांख्यिकीय विधियों के उपयोग के अभाव में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण असंभव है।
सांख्यिकी की विशेषताएं
(1) तथ्यों को आंकड़ों में प्रस्तुत करना
सांख्यिकी का संबंध किसी तथ्य को अच्छे या बुरे, सामान्य, सही या गलत आदि के रूप में प्रस्तुत करने से नहीं है, बल्कि प्रत्येक निष्कर्ष को प्रतिशत, अनुपात, औसत या विचलन के रूप में संख्याओं द्वारा दर्शाकर किया जाता है। वास्तविक अर्थ में, सांख्यिकी संख्यात्मक आँकड़ों का एक समूह है।
(2) सांख्यिकी तथ्यों का समूह है
सांख्यिकी का सम्बन्ध एक या दो या तीन आँकड़ों से नहीं होता, अपितु तथ्यों या निष्कर्षों के उस समूह पर आधारित समूह को सांख्यिकी कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम बहुत से लोगों की मासिक आय के आधार पर उन सभी की मासिक आय का औसत निकालते हैं, तो यह सांख्यिकी से संबंधित होगा।
(3) तुलना का आधार
सांख्यिकी से तात्पर्य उस आँकड़ों से है जो व्यवस्थित रूप से एकत्र किया जाता है। जिनकी आपस में तुलना की जा सकती है। ऐसी तुलना तभी संभव है जब तुलना की श्रेणियों में समरूपता या एकरूपता हो।
उदाहरण के लिए, यदि हम विभिन्न वर्गों की आय और उनकी शिक्षा से संबंधित आंकड़े एकत्र करें, तो उनकी तुलना की जा सकती है क्योंकि शिक्षा का सीधा संबंध लोगों की आय से है।यदि वृक्षारोपण डेटा के साथ व्यक्तियों की आय की तुलना की जाती है, तो उन्हें आँकड़ों में नहीं रखा जा सकता क्योंकि एकरूपता नहीं है। उपर्युक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि आंकड़ों के केवल वे समूह जो एक दूसरे से तुलनीय हैं, सांख्यिकी कहला सकते हैं।
(4) पूर्व निर्धारित उद्देश्य
सांख्यिकी की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इससे सम्बन्धित समक या आँकड़े एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए एकत्रित किये जाते हैं। ऐसे आंकड़े आकस्मिक और मनमाना नहीं हैं बल्कि सुनियोजित और बहुत व्यवस्थित हैं। बिना प्रयोजन के प्राप्त तथ्यों को हम अंक/संख्यांक कह सकते हैं। लेकिन उन्हें समक या आँकड़े नहीं कहा जा सकता।
उदाहरण के लिए, यदि किसी औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जाना है, तो जिस उद्देश्य के लिए तथ्यों का संग्रह किया जा रहा है, उसका उद्देश्य पहले से निर्धारित किया जाता है। इस लक्ष्य के लिए काम के घंटे, दैनिक मजदूरी, स्वास्थ्य की स्थिति, परिवार का आकार, शैक्षिक स्तर आदि जैसे तथ्यों को एकत्र किया जा सकता है।
(5) आँकड़ों की शुद्धता
सांख्यिकी में पर्याप्त शुद्धता की उपस्थिति सांख्यिकी की एक विशेष आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि अध्ययन के विषय की प्रकृति और शोध का उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए। आँकड़ों की शुद्धता विषय की प्रकृति और विशिष्ट स्थिति से संबंधित है। यह परिशुद्धता मात्रा या संख्याओं की संख्या से निर्धारित होती है जिसके आधार पर एक उपयोगी निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
(6) आँकड़ों का व्यवस्थित संग्रह
सांख्यिकी की एक प्रमुख विशेषता आँकड़ों का समावेश है जिसे व्यवस्थित रूप से संकलित किया जाता है, यदि कुछ आँकड़ों बिना किसी योजना के एकत्र किए जाते हैं, तो ऐसे समकों को सांख्यिकी नहीं कहा जा सकता है।
(7) विभिन्न कारकों से प्रभावित
एक विज्ञान के रूप में सांख्यिकी से संबंधित सांख्यिकी कई स्थितियों से प्रभावित होती है। सांख्यिकी का संबंध केवल एक पक्ष के विश्लेषण से ही नहीं है, बल्कि उन सभी कारकों के आंकलन अथवा विवेचन से भी है जो किसी विशेष स्थिति में परिवर्तन का कारण बनते हैं, साथ ही साथ घटनाओं के बीच सह-संबंध को व्यक्त करते हैं।
उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी विशेष समुदाय के जीवन स्तर से संबंधित समकों एकत्र करना है, तो ऐसी कई स्थितियाँ हैं जो जीवन स्तर से संबंधित आँकड़ों को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे कि विभिन्न अवधियों में वस्तुओं की कीमतें, लोगों की आदतें। रहन-सहन, व्यक्ति की मानसिक क्षमता और श्रम की प्रकृति।
(8) संगणना तथा निदर्शन के आधार पर
सांख्यिकी में निहित आंकड़ों का संग्रह कई विधियों और तकनीकों पर आधारित होता है। उद्देश्यपूर्ण विधियों द्वारा संकलित संगणना और प्रदर्शन आधारित डेटा सांख्यिकी की विशेषता को दर्शाता है। एक सीमित अनुसंधान क्षेत्र में, संबंधित संपूर्ण इकाइयों में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन करके आँकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है।
(9) सामान्य प्रवृत्तियों का अध्ययन
सांख्यिकी विशेष रूप से एक ऐसा विज्ञान है जो सांख्यिकी के आधार पर किसी विषय से संबंधित सामान्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट करता है। सांख्यिकी की मूल धारणा यह है कि कुछ संख्याओं के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष अन्य संख्याओं पर भी लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी विशेष समाज में काम करने की स्थिति, स्वास्थ्य स्तर, मासिक आय, जन्म दर, मृत्यु दर आदि जैसे आँकड़े एकत्र किए जाते हैं, तो उनके आधार पर जनसंख्या से संबंधित सामान्य प्रवृत्तियों को अन्य समानताओं के लिए समझा जा सकता है।
BY : TEAM KALYAN INSTITUTE
You can also check out these posts of ours 👇👇👇
Raksha Bandhan (Rakhi) Festival
Digital Inclusion Among Rural Minority Women